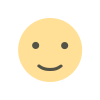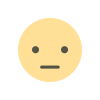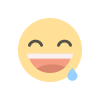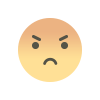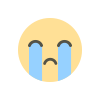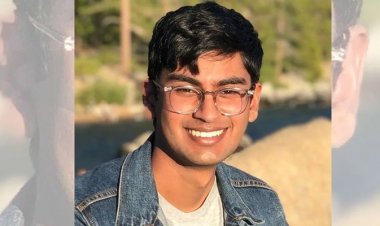साभार सद्विप्र समाज सेवा एवं सदगुरु कबीर सेना के संस्थापक सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की अनमोल कृति शिव तंत्र से
प्रदीप नायक प्रदेश अध्यक्ष सदगुरु कबीर सेना छत्तीसगढ़

विरोचन का राज्यारोहण
प्रहलाद ने देवेन्द्र की इच्छानुसार राज्य किया। इनकी अपनी नीति कुछ भी नहीं थी। यज्ञ से नीति तक सब शुक्राचार्य निर्धारित करने लगे। रक्ष संस्कृति के लोग दमन के शिकार बने। प्रह्लाद की प्रशंसा की गयी। पुराणों में इनकी प्रशंसा में स्तुति की गयी।
ये सम्मान पूर्वक से स्वर्ग के अधिकारी बने। प्रहलाद का राज्य भी अब देवेन्द्र का गढ़ बन गया। देवेन्द्र एवं देवर्षि लोग बिना रोक-टोक घूमने लगे। जब प्रह्लाद की उम्र ढलने लगी। इन्द्रिय सुख से जी ऊबने लगा। सत्यासत्य का भान होने लगा। झूठी प्रशंसा का भान होने लगा। तब देवेन्द्र एवं शुक्राचार्य ने सोचा कि प्रहलाद विरोध न करे, इससे अच्छा होगा कि उसे स्वर्ग भेज दिया जाये। तत्काल उसके पुत्र विरोचन का राज्यारोहण कर दिया गया, प्रहलाद को समझा-बुझाकर। उधर विरोचन को राज्यारोहण सुख दिखाकर मिला लिया देवेन्द्र ने। प्रह्लाद को अमृतपान कराकर पुनः युवा बनाने का एवं स्वर्ग का सुख भोगने का आश्वासन दिया गया। जिससे योजनानुसार प्रहलाद तैयार हो गये। विरोचन का राज्यारोहण शुक्राचार्य एवं देवेन्द्र की मदद से किया गया। जिससे विरोचन भी एहसान तले दबा रहे। विरोचन ने भी अपने पिता की तरह ही शुक्राचार्य से यज्ञ कराया। देवेन्द्र समेत सभी देवगणों को खुश किया। राज्य का अमूल्य कोष लुटाया। देवता लोगों ने कीमती सामान यज्ञ रूपी माध्यम से ग्रहण किया। यह समय भी अच्छा ही कहा जायेगा।

राजा बलि का राज्य
विरोचन की स्थिति देखकर साधारण जनता विद्रोह की स्थिति में आ गयी। उसे देवेन्द्र के जाल में फँसे देख जनता में घोर निराशा हो गयी। रक्ष संस्कृति के विद्यालय बन्द हो गये। ये हिंसा करना ही पाप समझते थे। अहिंसा के पुजारी थे। जीओ एवं जीने दो का सिद्धान्त मानते थे। वही प्रक्रिया उल्टी हो गयी। यज्ञ की आड़ में हिंसा करना ही पुण्य समझा जाने लगा। सोमरस का पान ही प्रगति का प्रतीक कहा जाने लगा। सामाजिक-पारिवारिक सम्बन्ध टूटते नज़र आये। उनका अपना भविष्य अन्धकारमय नज़र आया। इस स्थिति को विरोचन पुत्र बलि समझ गये थे। किसी भी चीज़ की अति होती है। इन परिस्थितियों में बलि चिन्तन-मनन करने लगे। अपने श्रेष्ठजनों से परामर्श करने लगे। मन-ही-मन देवेन्द्र के खिलाफ एवं पुनः रक्ष संस्कृति को स्थापित करने हेतु संकृत्य ले लिया। विरोचन को भी एवं भूल का एहसास हुआ। अतएव विदोवान के सति को अपने नाम से अपने अनुसार एक नगर बसाने का आदेश दे दिया। वियन के सोया कि अलग नगर इमर अपनी राजधानी वहीं हस्तान्तरित कर लेगा। बलि को राज्य का भार सौंप माकरत हो जाऊँगा। यह अपनी इच्छानुसार सभ्यता संस्कृति का विकास करें। चूंकि दो पुश्त को बरबादी सभी जनता के सामने थी। यह सब उसने अलग भूमि की खोज की। सोच-समझकर
राजा बलि की नीति
बलि ने वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक भू-खण्ड खोज दिया। नगर निर्माण का कार्य पूरा किया। उसी नगर में उनको राजगद्दी भी दी गयी। राजगद्दी के समय जब शुक्का चार्य को मालूम हुआ कि हमें बिना बुलाये यह कार्य हो रहा है जो ठीक नहीं हैं। वे खुद वहाँ पहुँचे। बिना मांगे आशीर्वाद देने लगे। शुक्राचार्य का यह अभिन्न अंग बन गया था। राजा को किसी तरह खुश रखो। बिना मांगे ही सही आशीर्वाद दो। कपटपूर्ण मंगल की कामना करो। बलि को यह सब ज्ञात हो गया था। बलि ने राजगद्दी पर बैठते ही कह दिया- मेरे राज्य में सभी सदाचारी होंगे। एक पली-धर्म के साथ तंत्र में निष्णात होंगे, ब्रह्मचारी होंगे। किसी भी तरह की हत्या नहीं होगी। मांस-मदिरा आज से बन्द होगी। शुक्राचार्य को यदि यहाँ रहना होगा तो हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को मानकर पठन-पाठन करना होगा। यज्ञादि बिना हिंसा के हमारे तंत्र विधि से यानी सदा शिव द्वारा दी गयी विधि से होगा। किसी भी तरह की देव संस्कृति अपने यहाँ नहीं चलने देंगे। हालाँकि देवेन्द्र से मेरा सम्बन्ध मित्रवत् वैसे ही होगा, जैसे दो राष्ट्राध्यक्षों का होता है। यज्ञादि उनकी इच्छानुसार नहीं होगा। जब अपने देश में वे अपनी ही संस्कृति रखे हैं तो हमारे यहाँ हस्तक्षेप करने का क्या कारण हो सकता है? हम किसी भी तरह से उनके ऋणी नहीं हैं। अतएव शुक्राचार्य अब नीति का निर्धारण आपके परामर्श से नहीं बल्कि रक्ष संस्कृति के जन-प्रतिनिधि के अनुसार होगा। जन-प्रतिनिधि ही वास्तविक जनता का राजा होगा। हम उन नीतियों का पालन करने में मदद करेंगे। जनता की सुख-सुविधा में जो भी खलल उत्पन्न करेगा, वह दण्ड का भागी होगा। हम किसी से भी किसी तरह भयभीत नहीं हैं। हमें भयभीत करने से बाहर की संस्कृति बाज आयें।
बलि के प्रथम दिन राष्ट्र को सम्बोधन ने शुक्राचार्य को हिला दिया परन्तु प्रतिष्ठा गवां कर भी कूटनीतिक दृष्टिकोण से रहना उचित ही समझे। बलि की वह राजधानी बलिपुर के नाम से विख्यात हुई। जो वर्तमान का बलिया है। यह उसी की यादगार में है। राजा बलि नीतिपूर्वक प्रजा की इच्छानुसार राज करने लगे। उन्होंने भानव संस्कृति के ऋषिगण को आमंत्रित किया। उन लोगों से सलाह-मशविरा कर राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हो चला। इनके नज़दीक ही विश्वमित्र भी रहते थे। जहाँ ये परामर्श लेना उचित समझते, मिल आते थे। राजा बलि की जय-जयकार होने लगी। प्रह्लाद के द्वारा खोई हुई प्रतिष्ठा राजा बलि वापस ले आये। कोई भी दुखी नहीं था। समता का राज्य था। सभी बराबर थे। सभी शारीरिक योग्यता के अनुसार कार्य करते एवं आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक मिलता। सभी शिव के तंत्र के साधक थे। प्रजा की इच्छानुसार बलि एक यज्ञ का अनुष्ठान कराने की सोचने लगे।

राजा बलि का यज्ञ एवं शुक्राचार्य की भूमिका
राजा बलि ने प्रजा के परामर्श से शुद्ध सात्विक यज्ञ, जैसा महर्षि विश्वमित्र करते थे, करने का निश्चय लिया। इस यज्ञ को करने वाले स्वयं बलि ही थे एवं विधि विशेषज्ञ रक्ष संस्कृति तथा मानव संस्कृति के ऋषिगण थे। इसमें किसी तरह की हिंसा नहीं थी। मदिरा का प्रावधान नहीं था। देवगण आमन्त्रित नहीं थे। देव संस्कृति के विषय में बहुत चौकन्ना थे-राजा बलि। परन्तु सत्य है कि नीति में ज्यादा उदार होना भी खतरनाक है जैसे अयोध्या के राजा उदारतावश वशिष्ठ को नहीं हटा पाये वैसे ही बलि शुक्राचार्य को। जिसका परिणाम बार-बार इन लोगों को भोगना पड़ा। शुक्राचार्य को राजा बलि के द्वारा इस यज्ञ में कोई खास भूमिका नहीं दी गयी। इससे शुक्राचार्य बहुत खिन्न थे। सारे तथ्यों को देवेन्द्र के सामने रखा। देवेन्द्र भी चिन्तित हो उठे कि ऐसा न हो कि वह इस यज्ञ से शक्ति अर्जित कर देव-लोक पर ही आक्रमण कर दे। देवेन्द्र ने देवर्षियों एवं स्वर्ग के पार्षदों को बुलाकर मन्त्रणा की। वे लोग इस निष्कर्ष पर पहुँच गये कि हम लोग किसी भी स्थिति में इस यज्ञ को नष्ट नहीं कर सकते हैं। चूँकि शुक्राचार्य यह बोल दिए थे कि उस यज्ञ मण्डप पर, उस राजधानी या उस नगर में देवताओं का प्रवेश करना वर्जित है। इसलिए देवेन्द्र हरि के यहाँ पहुँच गये। हरि से प्रार्थना की गयी कि राजा बलि बहुत ही प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति हैं। वे धर्म को भली-भाँति समझते हैं। तंत्र वेत्ता भी है। उसके बहुत प्रतिनिधि पाताल (अमेरिका) में भी अपना कार्यक्षेत्र फैलाने के लिए चले गये हैं। यदि उसका यह यज्ञ पूर्ण हो जाता है, तो यह सम्भव है कि स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दे। हरि कुछ काल तक सोचते रहे फिर शुक्राचार्य को निर्देशित करते हैं कि आप राजा बलि के यज्ञ मण्डप में पहुँच जाएँ। मैं अपना रूप बदलकर मानव संस्कृति के ऋषि-राज के भेष में पहुँच जाऊँगा। जैसा आप कहते हैं कि वह दानशील व्यक्ति हैं तथा यज्ञ में किसी के द्वारा कुछ भी माँगा हुआ वह पूर्ति करता है तो मैं उससे यह भू-मण्डल जिसका वह राजा है, ही माँग लूँगा। एवं आप तुरन्त संकल्प करा दीजियेगा। इसी मन्त्रणा के अनुसार शुक्राचार्य अपने गन्तव्य स्थल के लिए प्रस्थान कर जाते हैं एवं हरि भारतीय संन्यासी के रूप में सिद्धाश्रम पहुँचते हैं। जहाँ से यज्ञ के निमित्त प्रतिदिन याज्ञिक लोग जाया करते थे। हरि भी उन्हीं लोगों के साथ हो लिए। जब राजा बलि दान के लिए साधुओं ऋषियों को आमन्त्रित करते हैं तो उस दिन दान लेने वालों में मात्र छद्म वेषधारी हरि ही थे। यह शुक्राचार्य की व्यवस्था थी। जबकि सिद्धाश्रम में एक पुरोधा ने राजा बलि से बता दिया था कि आज दान में आपके साथ छल किया जायेगा। हम लोगों के साथ आने वाला व्यक्ति वह हमारे आश्रम का ऋषि नहीं, छद्म वेषधारी कोई अन्य मालूम होता है। यहाँ की व्यवस्था देखने पर मालूम होता है कि वह शुक्राचार्य का आदमी है। राजा बलि सोचते हैं कि चाहे जो कोई हो दान ही तो लेगा। दान देकर उसे सन्तुष्ट कर दिया जायेगा। हरि राजा बलि से दान की याचना करते हैं। राजा बलि हरि की रूप रेखा देखकर सहज ही यह अन्दाज लगा लेते हैं कि यह रूप-रंग देव प्रतिनिधि का नहीं हो सकता है क्योंकि वे लम्बे और नुकीले नाक वाले सुन्दर होते हैं पर यह तो नाटा कद का सांवले रंग का भारतीय संन्यासी ही होगा। अतएव इस पर अविश्वास करना उचित नहीं है। राजा बलि कहते हैं संन्यासी मांग लो ! तुझे क्या माँगना है? छद्म वेशधारी हरि नम्र रूप में कहता है-महाराज की जय हो ! मुझे इस पृथ्वी पर रहने की कोई जगह नहीं है एक छोटा-सा आश्रम बनाने हेतु कुछ भूमि दान दे दें। राजा ने तथास्तु कह दिया। फिर राजा बोले तुझे कितनी ज़मीन चाहिये। हरि प्रत्युत्तर दिए, महाराज। आप तो ज़मीन दान दे ही दिए। अब उसका संकल्प अपने पुरोहित शुक्राचार्य द्वारा करायें। शुक्राचार्य संकल्प हेतु कुशा एवं जल लेकर कहे कि राजन् लो संकल्प करो। दान से व्यक्ति की कीर्ति बढ़ती है। राजा बलि को सोचने का समय नहीं दिया तथा उस याचक के आश्रम हेतु उनकी राजधानी ही शुक्राचार्य ने संकल्प करा दी। जब राजधानी संकल्प करा दी गई तो वहाँ के याज्ञिक राजा बलि से बोले, महाराज! यह तुमने क्या कर दिया? शुक्राचार्य ने तो छल से तुम्हारी राजधानी का संकल्प करा दिया। तब हरि प्रसन्न मुद्रा में राजा को आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि हे राजन् तेरा मंगल हो, तुम्हारे द्वारा दिए गये दान से मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ। उम्मीद है तुम यह जगह शीघ्र ही खाली कर दोगे। जिससे मैं यहाँ कुटिया बना सकूं। राजा को अपने छले जाने का एहसास हुआ तथा समन्न गये कि यह व्यक्ति शुक्राचार्य के आमन्त्रण पर आया हुआ कोई और नहीं, देवेन्द्र या हरि हो सकता है। राजा बलि ने कहा देवर्षि तुम महर्षि का रूप क्यों पकड़े हो। क्या दान भी लिया जाता है छल से ? तुम लोग अपना राज तंत्र बढ़ाने के लिए किसी भी साधन का उपयोग कर सकते हो। यह उचित नहीं प्रतीत होता है। हरि चतुर एवं वाक्पटु तो थे ही तुरन्त बोल उठे क्यों राजन् संकल्प के द्वारा दिया वचन भी वापस लेना चाहते हो। क्यों शुक्राचार्य-यही आप कहते थे कि आपका यह यजमान वचन का धनी एवं अद्वितीय दानी है। क्या दिए हुए दान पर भी तर्क-वितर्क होता है? राजा बलि स्वाभिमानी थे, सत्यव्रती थे। अतएव अपने द्वारा बसाये हुए नगर बलिया का परित्याग कर पाताल-लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। वह पाताल यानी अमेरिका महादेश का भू-भाग।

बलि के यज्ञ का आध्यात्मिक महत्व
राजा बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्र का अर्थ होता है वीर्य ग्रहण करने की कला। जो इस कला को जानता है वही अमरत्व को प्राप्त करता है। इस कला को शुक्राचार्य ने संजीवनी तंत्र (विद्या) कहा। परन्तु यह तंत्र पूर्णत्व, ब्रह्मत्व, बुद्धत्व को नहीं उपलब्ध करा सकता है। चूँकि अमरत्व से बुद्धत्व का कोई सम्बन्ध नहीं है।
राजा बलि अपने गुरु के निर्देशन में यज्ञ कर रहा है। जगत के विस्तार के लिए। अर्थात् मूलाधार चक्र ही संसार विस्तार का प्रतीक है। खैर साधक किसी भी तरह का शुभ कार्य करता है तब उसे सद्गुरु मिल ही जाते हैं। उसमें पात्रता आ ही जाती है।
भगवान वामन का अवतार सिद्धाश्रम (बक्सर) में ही मानव संस्कृति में होता है। अवतार एवं सद्गुरु विश्व कल्याण की कामना से ही आते हैं। वे राजा बलि से दान माँगने के लिए उसके यज्ञ में पहुँचते हैं। उसके पहले ही राज पुरोहित, कुल गुरु राजा को सावधान करता है। एक भिक्षुक आयेगा। तुम उसे दान मत देना। पुरोहित सदैव अपने हित का चिंतन करता है। वह पुश्त-दर पुश्त यजमान को नहीं छोड़ता है। यजमान ही उसकी खेती है। सम्पत्ति की तरह वह बंटवारा करता है। यजमान पर निर्भर करता है कि वह कैसे इनसे मुक्त हो सकता है। राजा बलि के सामने भिक्षुक आता है। "भिक्षां देहि!" की आवाज देता है। बलि उन्हें अपने घर पर ले जाते हैं। पाद प्रक्षालन के पश्चात् पति-पत्नी आरती कर भोग लगाते हैं। फिर निवेदन करते हैं कि प्रभु माँगो, क्या माँगते हो ? उसकी पुत्री उस वामन भगवान को देख कर कामना करती है कि तुम्हें मेरा पुत्र होना चाहिए।
भगवान कहते हैं कि राजन! मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा था तब रास्ते में एक दुकान के सामने संध्या वंदना करने लगा। इतने में दुकानदार आ गया। अपनी दुकान खोलने हेतु उसने मुझे वहाँ से हटा दिया। अतएव मुझे एक झोपड़ी हेतु जगह चाहिए।
राजा ने कहा- आप मेरे राज्य में कहीं भी झोपड़ी लगा सकते हैं। इसके लिए क्या माँगना था। नहीं राजन ऐसा नहीं कर सकता। मैं नैमिश्टिक ब्रह्मचारी संन्यासी हूँ। मैं लोभ लालच नहीं करता हूँ। तुम मुझे साढ़े तीन कदम पृथ्वीदान कर दो। राजा ने अपने गुरु को बुलाया। वह आते ही पहचान गये। उन्होंने कहा राजन । इसे जमीन मत दो। यह छल करेगा। तुम्हारा अस्तित्व समाप्त कर देगा। परन्तु राजा बलि में भक्त प्रह्लाद का खून था। वह आज दे ही देना चाहते थे। गुरु संकल्प कराने से इनकार कर देते हैं। भगवान ने कहा- तुम अक्षत जल दो, मैं संकल्प का मंत्र बोल देता हूँ। जब शुक्राचार्य ने देखा कि शिष्य हाथ से निकलने वाला है तब वह यज्ञ के जल पात्र के छिद्र में प्रवेश कर जाते हैं। जिससे जल ही नहीं निकलेगा। न ही संकल्प पूरा होगा। वामन भगवान कुशा से छिद्र साफ कर देते हैं। जिससे गुरु जी की एक आँख फूट जाती है। संकल्प पूरा होता है। अब वे पर्वतांकार आकार ग्रहण कर लेते हैं। एक पद में सम्पूर्ण पृथ्वी, दूसरे में आकाश, तीसरे के लिए माँग करते हैं, इसके लिए बलि अपने शरीर को प्रस्तुत करते हैं। यह देख उनकी लड़की को क्रोध आता है। वह वामन को मारने का संकल्प लेती है। परन्तु बलि पूर्ण
समर्पित भाव से अपने को प्रस्तुत करता है। जब शिष्य अपना तन-मन-धन सद्गुरु को निर्विचार भाव से समर्पित कर देता है। तब सद्गुरु शिष्य का रजो गुण, तमो गुण, सतो गुण हरण कर लेता है। उसमें स्वयं प्रवेश कर जाता है। उसके मस्तक पर एक पैर रखता है, एक पैर उसके पैर पर। अर्थात मूलाधार से उसके कुण्डलिनी को क्षण भर में सहस्त्रार तक पहुँचा देता है। जिससे ज्ञान-भक्ति रूपी गंगा प्रवाहित होने लगती है। बलि अब कर्म-काण्ड से मुक्त हो गये। वे उपलब्ध हो गये विष्णु स्वरूप को। यही है, विष्णु तंत्र।
सद्गुरु के सामने जो भी संकल्प भूल कर भी लेंगे वह उसे पूरा कर देता है। उसकी लड़की ही कृष्णावतार में पूतना बनी। जो पुत्रभाव रखी थी। अतएव स्तनपान कराने पहुँची। फिर उसकी हत्या का संकल्प लिया, अतएव राक्षसी रूप में हत्या का प्रयास भी किया। परन्तु उस परम पुरुष से ही किया अतएव उसे भी अपने स्वरूप को प्रदान किया।
राजा बलि ने पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया परन्तु उनकी पूर्व कामना थी राज्य की अतएव इस को भोग लेना ही उचित समझा। अतएव नारायण ने पातालपुरी का राज्य सौंप दिया। पाताल अर्थात् मूलाधार ही पाताल का प्रतीक है। सांसारिक राज्य यही होगा परन्तु अब वे निवास करेंगे सहस्त्रार पर। कैलाश पर। वहीं गंगा शिव की जटा मैं प्रवाहित होती है। ज्ञान ही गंगा है। जो आपके शिव अर्थात सहस्त्रार पर प्रवाहित होता है। नारायण ने मानव रूप में ही सद्गुरु बन कर राजा बलि को वैष्णव तंत्र में दीक्षित कर, उनका उद्धार किया।
वैष्णव धर्म
देवेन्द्र अत्यन्त प्रसन्न होते हैं तथा तत्क्षण देवर्षि एवं अन्यान्य पार्षदों, देवताओं, अप्सराओं के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं तथा हरि के सम्मान में सोमयज्ञ प्रारम्भ कर देते हैं। यह यज्ञ बृहस्पति के द्वारा पूर्ण किया जाता है। इस तरह इस भू-भाग पर भी देवताओं के द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिया गया। हरि को इधर आना एवं कुछ काल निवास करना अत्यन्त सुन्दर लगा। अतएव ये यहीं तप करने लगे।
हरि का तप क्षेत्र था बलिया का भू-भाग। यहीं से रस-प्रधान तंत्र की व्यवस्था की। जिसका प्रचार-प्रसार इसी भू-भाग से किया, जिसे वैष्णव तंत्र कहा गया। इसमें भाव को प्रधानता दी गयी। इसमें क्रिया को गौण रखा गया। भावना को प्रभुसत्ता दी गयी। चाहे जहाँ हो जिस अवस्था में हो। भावना को परम-पुरुष के साथ लगा देना है। सोचना है मैं उसी के साथ हूँ। जो कुछ हो रहा है उसी के इच्छनुसार होता है। मैं तो उसके ही निमित्त हूँ। स्नान, ध्यान, पूजा पाठ उसी के साथ, इस भावना के साथ तादात्म्य स्थापित किया गया। यही था वैष्णव धर्म। बाद में इसका भी रूप विकृत होता गया। देव संस्कृति की ज्यादा सामीप्यता के चलते इसमें भी बाह्य पार्थिव पूजा की महत्ता आ गयी। कर्मकाण्ड पकड़ लिया। चूँकि देवर्षिगण का आगमन इस धर्म में ज्यादा हुआ। अतएव कालान्तर में विष्णु की भी काल्पनिक मूर्ति बनने लगी। उसके पीछे देवेन्द्र इत्यादि देवता पुनः आ गये। अब पार्थिव पूजन का आविष्कार हो गया। इसकी व्याख्या शास्त्रों में कर दी गयी। इसमें भी पुण्य-अपुण्य की चर्चा की गयी। इस तरह इसका प्रचार अगस्त्य ने भी दक्षिण में करना शुरू कर दिया। दक्षिण में यही भावना प्रधान के आधार पर कालान्तर में भक्ति का उदय हुआ। इसी से भक्ति का जन्म स्थान दक्षिण ही माना जाता है।
हरि अब पूर्णरूपेण विष्णु बन गये। विष्णु नाम से उनकी चर्चाएँ होने लगीं। पुराणों में विष्णु का वर्णन होने लगा। आप सहज ही अन्दाजा लगा सकते हैं कि ऋग्वेद कब का है, पुराण कब का है। यह अन्दाजा साहित्य के शब्दों एवं रचना से लग जाता है कि किस काल में कौन-सी रचना, शैली, शब्दों का प्रचलन था। वास्तविक वैष्णव वह है जो प्रत्येक कण में अपने प्रभु का दर्शन करता है। यह विराट उस विष्णु का ही विस्तार है। इस तंत्र को जानना ही वैष्णव तंत्र है। फिर वह साधक स्वयं विष्णुमय हो जाता है। शरीर से जो कुछ किया जाय वह योगासन है। मन से जो कुछ किया जाये वह ध्यान है। जब साधक आत्मा में स्थित हो जाता है तब भक्ति तंत्र का आविर्भाव होता है। आत्मा के परमात्मा में मिलने की कला ही वैष्णव तंत्र है। कर्मकाण्ड ही देव तंत्र है।
भृगुऋषि का पदार्पण
विष्णु पुनः अपने नागीय भवन में चले गये। देवेन्द्र वगैरह को यह भ्रम हो गया कि विष्णु अब बिल्कुल शान्त हो गये। देवगणों या मानव ऋषि से कोई खास रुचि नहीं रखते। क्या उनका क्रोध ही समाप्त हो गया? क्या अब वे अपने को इस मध्य धारा से अलग रखना चाहते हैं? इत्यादि प्रश्न उनके मन में उठते थे। उन सब लोगों ने उनकी भावना जानने हेतु भृगुऋषि को उनके निवास स्थान पर भेज दिया। भृगु ने उनसे नाना प्रकार के प्रश्न किये। वे शान्तचित्त उनके प्रश्नों का उत्तर देते रहे। हर समय भावना को परम-पुरुष में ही रखने को कहते। इससे क्रोध नहीं आता । इन्द्रिय वृत्ति धीरे-धीरे शान्त होगी। इस भावना से दमन नहीं होता। परिवर्तन होता है। भृगुऋषि को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे हर समय कर्मकाण्ड, यज्ञादि पर ही जोर दे रहे थे। इन परिस्थितियों में भृगु को क्रोध आ गया। जब आदमी को अहंकार, क्रोध आता है तो किसी का ख्याल नहीं होता। उसका विवेक हर जाता है। क्रोध से पराजित व्यक्ति हांफने लगता है। श्वास तेज चलने लगती है। जब कहीं आग लगती है, तो हवा जोरों से चलने लगती है। चूँकि वहाँ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगती है। इसी तरह अन्दर भी व्यक्ति जब 'स्व' का दहन करता है। श्वास तेज़ चलता है। इसी से विवेक खो देता है वह। भृगु ऋषि भी क्रोधावेश रोक नहीं सके। क्रोध का अन्तिम फल होता है थूक देना या मार देना। भृगु ने भी क्रोधावेग में विष्णु की छाती में जोरदार लात जड़ दी। विष्णु शरीर मन से सशक्त थे। वे भृगु का पैर पकड़ कर कहने लगे- हे मुनिवर आपको कहीं चोट तो नहीं आयी। आप तप करने वाले जो ठहरे, मैं तो लड़ाकू कौम से आता हूँ। युद्ध करता हूँ। मारना-मरना तो मेरा कर्तव्य है। आप कैसे कर दिए? कहीं आपको चोट तो नहीं आ गयी। भृगु का क्रोध उसी तरह शान्त हो गया जैसे जलती हुई अग्नि पर शीतल जल गिरे। भृगु लज्जित हो गये। क्षमा याचना करने लगे। जब व्यक्ति साधारण अवस्था में रहता है तो श्वास की गति भी सामान्य हो जाती है।
विष्णु ने कहा कि हे मुनिवर। आपका दोष नहीं है। आपकी भावना ही कुछ ऐसी हो गयी कि आप क्रोध से बुरी तरह पराजित हो गये। आप अपने को संयमित रखें। भावना को परम-पुरुष में रखते हुए मनन करें। फिर तो आप मुनि हैं ही। इस तरह विष्णु भृगु को वैष्णव तंत्र में दीक्षित कर भक्ति करने का आदेश दे देते हैं। उनके द्वारा भक्ति के निमित्त स्थान पूछने पर उन्हें वहीं बलिया भेज देते हैं। जहाँ भृगु तप करने लगे। आज भी भृगुऋषि का आश्रम वहाँ मौजूद है।
जालंधर
विष्णु के द्वारा प्रतिपादित वैष्णव धर्म दक्षिण-पश्चिम भाग में भी फैलने लगा। किसी भी संस्कृति का नाश नहीं होता। दब जाती है परन्तु समय पाकर पुनः पल्लवित-पुष्पित हो जाती है। इसी सन्दर्भ में रक्ष संस्कृति का एक उपासक और सामने आता है। जो अत्यन्त, उदार, धर्म प्रवीण यौद्धा था, तप के द्वारा शिव को खुश कर लिया था। तंत्र का अद्वितीय ज्ञाता हो गया था। उसकी प्रजा भी तंत्र सम्पन्न थी। दोनों पति-पत्नी तंत्र विधि से अपने में आनन्दित थे। पत्नी अत्यन्त ही पतिव्रतधर्म में लीन थी। यह सब देव संस्कृति के लिए आश्चर्य का विषय होना स्वाभाविक है। जैसे आज भी पश्चिम की औरतें भारतीय पतिव्रत धर्म की हँसी उड़ाती हैं। इसे मूर्खता का परिचायक मानती हैं। वे आज इसके साथ तो कल दूसरे और के साथ, नाजायज पुत्रों की बाढ़ लेकर आयी हैं। जिसके चलते समाज व्यवस्था ही चरमरा उठी है। उसी की नकल पूर्व भी कर रहा है। यहाँ भी महानगरों मैं वही स्थिति आती जा रही है। पति एवं पत्नी का धर्म भी कुछ होता है। ये जानते ही नहीं। ये कहते हैं हम Life-Partner की तरह हैं। जितना दिन चलता है, ठीक है, अन्यथा हम अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। मेरे एक मित्र आज के देव भूमि पश्चिम के पाताल लोक या नाग गन्धर्व भूमि अमेरिका गये थे। इन्हें एक निमन्त्रण मिला कि स्वामी जी आप अमुक जगह अमुक तारीख को अमुक समय आयें। वे बोले क्या है भाई। वहाँ के लोग जो कुछ पूर्व की तरफ मुखातिब हो रहे थे। समझाये कि स्वामी जी ये हैं भद्रपुरुष जो अपनी पत्नी के साथ लगातार 10 वर्षों तक रह गये। वही शादी की दसवीं वर्ष गांठ मनानी है। स्वामीजी कहे यह कौन अनहोनी है? वे भद्रपुरुष बताये कि स्वामी जी यह एकदम अनहोनी है। यहाँ तो साल दो साल किसी तरह एक साथ रह लेते हैं अन्यथा दो-चार माह में ही एक-दूसरे को छोड़ देते हैं। यहाँ के लिए यह शादी तो उदाहरण है कि दस साल तक एक साथ रह गये। यही है पति-पत्नी का सम्बन्ध ।
जालंधर के राज्य में सभी अपने-अपने धर्म में अवस्थित थे। यह देख कर देवेन्द्र चिन्तित हो उठे। जालंधर को भ्रष्ट करने हेतु पहले देवर्षि को भेजा गया। देवर्षि जब सफल नहीं हुए तब नारद स्वयं अपने गण-पार्षदों के साथ गये। जब वह किसी भी तरह के लालच में नहीं आये तो अपनी नीति के अनुरूप छल, बल, दाम, दण्ड, विभेद अपनाते हुए उस पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में इन्द्र हार कर भागे। सारे देवगण भयभीत होकर विष्णु के पास पहुँचे। उनसे अपनी व्यथा सुनाये। विष्णु देवेन्द्र की बातों पर विशेष ध्यान देने ही लगे थे। चूँकि उनका निवास एवं पत्नी लक्ष्मी भी उन्हीं के क्षेत्राधिकार में थी। विष्णु देवर्षि एवं देव को प्रसन्न करने हेतु युद्ध का नियम बनाये। उसे परास्त करने हेतु तरकीब सोचे।
जालंधर की पत्नी को भ्रष्ट करना
विष्णु ने उसकी कमजोरी का पता लगाने हेतु नारदीय व्यवस्था को उसकी राजधानी में भेज दिया। गुप्तचर लोग अपना रूप बदलकर काम करने लगे। विष्णु चढ़ाई कर दिए। जालंधर से घोर युद्ध होने लगा। हर बार विष्णु को पीछे धकेलते रहा। इससे विष्णु अत्यन्त चिन्तित हुए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें इतनी शक्ति आती कहाँ से है? प्रतिदिन नया ओज, नया जोश लेकर युद्धभूमि आता। सभी देव संस्कृति के लोगों पर कहर ढाल देता है। यह तो अजेय मालूम होता है। इसी बीच नारदीय व्यवस्था (गुप्तचर) के माध्यम से सूचना मिली कि इसकी पत्नी अपूर्व पतिव्रता है। इसके युद्ध में जाते ही उसी के ध्यान में स्थिर हो, परम-पुरुष को प्रार्थना करती है। हे परम पुरुष आप मेरे पति की रक्षा करें। जब तक उसका पतिव्रत धर्म ऐसा ही दृढ़ रहेगा। तब तक उसको मारना सम्भव नहीं है। विष्णु ने उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट करने हेतु आदेश दिया। जो भी देवगण या देवेन्द्र या देवर्षि अपना रूप बदल कर गये। वह उसके पतिव्रत धर्म के सामने टिक नहीं सके। उन्हें उल्टे पाँव लौटना पड़ा। उस औरत में विचित्र था-तेज। विचित्र था-नारीत्व। हर श्वास थी परम-पुरुष के लिए। अब उसका अमंगल कौन कर सकता है? पंजाब प्रान्त में जालंधर शहर इसी के नाम पर बसा है। जहाँ सती वृंदा का छोटा मंदिर आज भी है। आज भी उसकी आत्मा इसके इर्द-गिर्द घूमती है। आप चाहें तो वहाँ ध्यान करके उसकी आत्मा को निमंत्रित कर बातें कर सकते हैं। सच्चाई जान सकते हैं।
इस विचित्र परिस्थिति में विष्णु एक दिन उसकी पत्नी वृंदा के समीप गये। जब दूर से देखे तो समझ गये कि यह तपस्वनी है। इसकी पूरी चित्तवृत्तियाँ ध्यान पर ही हैं। परम-पुरुष पर ही अन्तर्मुखी हैं। अतएव पहले इसे बहिर्मुखी करना श्रेयस्कर होगा। विष्णु झट से अपना रूप बदलकर जालंधर का रूप धर लेते हैं। उधर युद्धभूमि में देवेन्द्र संभाल रहे हैं। विष्णु नकली जालंधर बन वृंदा के समीप जाते हैं। वृंदा झट-पट उठ खड़ी होती है। पूछती है- हे नाथ! आज आप इतना पहले क्यों आ गये ? विष्णु कहते हैं है प्रिय ! आज एकाएक तुम्हारे प्रति मन में अनुराग उत्पन्न हो गया। बरबस युद्ध से वापस आ गया। विष्णु ध्यान बहिर्मुख करने में समर्थ, चतुर थे ही। यही मौका उचित देख उसका सतीत्व भंग कर देते हैं। जब वह जाने को उद्यत होते हैं। तब वह पहचान जाती है कि यह तो कपटी, छली विष्णु हैं।
वृंदा का श्राप
वृंदा क्रोधित हो जाती हैं। कहती हैं है विष्णु क्या यही धर्मात्मा कहलाता है। यह कैसा धर्म ? हर समय, हर किसी से छल-कपट करना ही तुम्हारा धर्म है। दूसरी औरत से इस तरह का व्यवहार तू भविष्य में कभी न करना, जिससे हमारी दूसरी बहन का सतीत्व खतरे में पड़ जाये। मैं तुझे श्राप दे रही हूँ। इससे तुझे कोई नहीं बचा पायेगा। जाओ, तुम पत्थर हो जाओ। तुम्हारी गुप्तेन्द्रिय गिर कर पत्थर हो जायेगी। पौराणिक उल्लेख मिलता है कि वे पत्थर हो गये। वही देवेन्द्र के द्वारा पूजित शालीग्राम कहलाये। इधर सतीत्व नष्ट होने से जालंधर मारा गया।
वृंदा ने अपना शरीर अपने तेज़ से छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने किए पर पश्चाताप् करते हुए वृक्ष का रूप ग्रहण कर लिया। जो वृक्ष बाद में बहुत फैल गये एवं वृंदावन कहलाये। इस घटना को देखकर मानव-रक्ष संस्कृति के लोग दहल गये। क्या यही है देवत्व? क्या यही है अस्तित्व गत-बोध ? क्या यही है विष्णु का वैष्णव धर्म ? सभी गमगीन थे। परन्तु उसी की स्मृति में रक्ष एवं मानव संस्कृति के लोगों ने वृंदा को शुभ माना। अपने-अपने घर में लगाया। उसकी पूजा होने लगी। वह श्रद्धा की दृष्टि से देखी जाने लगी। वह संस्कृति की प्रतीक बन गयी। लोगों के मन-मस्तिष्क में इतना घर कर गयी कि उसके बिना घर ही सूना होने लगा। वृंदा का पत्ता पूजा-पाठ में, भोजन में, यज्ञादि में पड़ने लगा। किसी भी तरह का कार्य हो चाहे वह शुभ या मरते वक्त अशुभ हो वृंदा को अवश्य याद करते। यही वृंदा कालान्तर में तुलसी कहलायी। इसका आचरण व्यवहार सतीत्व इतना आदरणीय लगा कि मानव संस्कृति के लोगों ने इसकी लकड़ी को गले से लगा लिया। जिसे कण्ठी कहते हैं। इसे माला के रूप में धारण कर लिया। यह वृंदा के तप-त्याग का प्रतीक है। जिसे अभी तक मानव संस्कृति के लोग गले से, हृदय से लगाते हैं।
वैष्णव मत इससे आगे नहीं बढ़ पाया। चूँकि विष्णु का चरित्र देवेन्द्र से जुड़ गया था। देवेन्द्र एवं देवर्षि हेय दृष्टि से देखे जाते थे। अतएव वैष्णव धर्म आगे बढ़ते-बढ़ते रुक गया। शैव तंत्र का ही विकास सर्वत्र हुआ। बाद में विश्वमित्र का दिया हुआ गायत्री छन्द का। साहित्य का इतिहास देखने पर भी मालूम होता है कि वैष्णव धर्म का दक्षिण में पुनः ग्यारहवीं सदी में प्रचार शुरू हुआ एवं बारहवीं सदी तक जोर पकड़ा। इसमें देवी-देवताओं का अविर्भाव हुआ। इसी धर्म के साथ आयीं 84 लाख योनियाँ। कर्म फलाफल। एक तरफ तो इसने 12वीं सदी में भक्ति का आन्दोलन सा खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ पाण्डित्य का भी। खैर हम लोग हिन्दी साहित्य एवं भक्ति काल के इतिहास की तरफ जाने लगे। अतएव तंत्र पर पुनः सोचें।
माली एवं माल्यवान के द्वारा रक्ष संस्कृति को बचाना
येन-केन-प्रकारेण मानव संस्कृति देव संस्कृति से प्रभावित होने लगी। खासकर चन्द्रवंशी राजा ज्यादा प्रभावित हुए। ये सबल सशक्त होते थे। देवगण भी इनसे मधुर सम्बन्ध स्थापित करना चाहते थे। इसी वंश के एक और राजा नहुष थे जो देवेन्द्र को हटाकर कुछ काल तक देवेन्द्र के स्वर्ग का सुख भोगे। पुराणों में उनका भी कुछ अप्सराओं से सम्पर्क आता है। इस तरह बार-बार अप्सराओं के सुख, शराब के सुख की खोज में स्वर्ग के इर्द-गिर्द चक्कर काटने लगे। मानो मानव संस्कृति के दूषित होने का यही समय था। हालांकि इसी वंश के ज्यादा-से-ज्यादा लोग ऋषि भी हुए हैं। जिनका वर्तमान समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इन वंशों एवं ऋषियों का वर्णन आगे किया जायेगा। उनका प्रभाव देखते हुए रक्ष संस्कृति का चिन्तित होना स्वाभाविक था। रक्ष संस्कृति यानी राक्षस सिमटते जा रहे थे। देव संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। रक्ष संस्कृति के बचे मनीषी भी आरण्यों में छिपकर तप करने लगे। अपनी रक्षार्थ सोच विचार करने लगे। दक्षिणी भू-भाग के समुद्रीय तट पर रह रहे माली, सुमाली माल्यवान की स्थिति भी दयनीय हो गयी थी। देवगणों ने उन्हें भी विभिन्न प्रकार की लड़ाइयों में फँसाकर उनके अस्तित्व पर ही हमला बोल दिया था। माल्यवान अपने परिवार के साथ यत्र-तत्र भटक रहा था। उसे कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा था कि किस प्रकार देव संस्कृति से अपनी रक्षा की जाये। अन्ततोगत्वा देवर्षि पुलस्त्य, अगस्त्य का आधिपत्य हो गया था। वे नीति निर्णायक थे। वे बहुपत्नीक थे। इन्हीं के वंशजों का वर्चस्व था। देवेन्द्र भी इन्हीं के परामर्श के अनुसार कार्य सम्पादन करते थे।
लंका
उस समय रामेश्वरम से कुछ ही दूरी पर एक टापू था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नदियां अपना रास्ता बदलती रहती हैं। कभी दायें काटतीं तो कभी बायें भू छोड़ी। इसी तरह समय-समय पर समुद्र से भी टापू निकलता रहता है। उसी तरह का दक्षिण में एक सुन्दर टापू निकल आया था। देवेन्द्र एवं देवर्षि ने उस टापू का विकास किया। देवगण ने सोचा कि इस टापू से ही अपनी संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया जायेगा ? चूँकि स्वर्ग इधर से काफी दूर पड़ता है। अतएव इसे लघु स्वर्ग के रूप में विकसित किया गया। सारी सुख-सुविधाओं का जुगाड़ किया गया। मानव संस्कृति एवं रक्ष संस्कृति से लूटा गया धन यहीं लगाया गया। दोनों संस्कृतियों की सुन्दर अच्छी लड़कियों को भी लाया गया। चूँकि युद्ध जीतने के बाद इनका भी लूट-पाट करने में वर्तमान मुस्लिम शासकों की तरह ही व्यवहार था। अतएव उस टापू का विकास विश्वकर्मा नामक देव अभियन्ता की देख-रेख में सम्पन्न हुआ। दास-मजदूरों के रूप में दोनों संस्कृति के लोग बहु-संख्यक मात्रा में उपलब्ध थे ही। इन दोनों संस्कृतियों की लूट की सम्पत्ति को उस छोटे से टापू के विकास में लगा दिया गया। मात्र चन्द देवगणों के सुख का साधन यह टापू अब स्वर्ग से भी अच्छा लगने लगा। यहाँ अस्त्र-शस्त्र की खोज भी होने लगी। यहाँ से स्वर्ग पहुँचने के लिए विमान की भी आवश्यकता आ गयी। वह भी ऐसा विमान जिसपर आरुढ़ होकर ज्यादा-से-ज्यादा देवगण एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। युद्ध की निगाह से सामरिक भी हो। इस तरह विश्वकर्मा एवं बृहस्पति की मदद से एक विमान भी बनाया गया जिसे पुष्पक विमान कहा गया। इसका आकार बाहर से देखने में कमल पुष्प की तरह था। इसलिए इसे पुष्पक विमान कहा गया। इस टापू का ही नाम कालान्तर में 'लंका' पड़ा। यह अत्यन्त सुन्दर था। लंका के सब घरों पर स्वर्णाकृति कला थी। इसी से इसे सोने की लंका भी कहा गया। यह बहुत माने में स्वर्ग से भी ज्यादा सुरक्षित थी। सुख-साधन भी वहाँ से ज्यादा उपलब्ध कराये गये। यहाँ अन्वेषण का कार्य जोर-शोर से शुरू किया गया। देवेन्द्र यहाँ स्थायी रूप से रह नहीं सकते थे। अतएव लंका के संचालन के लिए उपयुक्त व्यक्ति की खोज करने हेतु पुलस्त्य को कहा गया। देवर्षि पुलस्त्य ने उचित समय एवं सुअवसर देख देवेन्द्र से अपने ही नाती 'कुबेर' के सम्बन्ध में कहा। देवेन्द्र को कुबेर भी ठीक ही जंचा। वहाँ बहुत दिनों से देव संस्कृति के प्रचारक के रूप में पुलस्त्य अपने एवं अपने बच्चों के साथ रहे थे। अतएव सर्व सम्मति से कुबेर को वहाँ का प्रमुख संचालक नियुक्त कर दिया गया।
कुबेर को लंका का राजा बनाना
अब कुबेर ने लंका के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया। उनकी छत्र-छाया में प्रचार तंत्र पर जोर दिया गया। देवज्ञ यज्ञ का विधान, देवज्ञ चमत्कार का प्रचार दक्षिण में अब जोर पकड़ गया। लंका में प्रथम बार विभागों का बँटवारा किया गया। जैसे प्रचार तंत्र विभाग, युद्ध तंत्र विभाग, अन्वेषण तंत्र विभाग, रक्षा तंत्र विभाग, गुप्तचर तंत्र विभाग, विधि-व्यवस्था तंत्र विभाग, गृह तंत्र विभाग, इत्यादि का वर्गीकरण कर कार्य का संचालन शुरू हो गया। यही कारण है कि उस समय की सबसे विकसित जगह, समुन्नत जगह एवं धन-धान्य से पूर्ण जगह का नाम था 'लंका'। अब देवतागण उत्तर से दक्षिण तक छा गये। वे निर्भय होकर घूमते। छोटे-छोटे जनपद जहाँ मानव ऋषि तप करते उनसे छेड़-छाड़ करना अब उचित नहीं समझते थे।
माल्यवान का पुलस्त्य आश्रम में शरण लेना
माल्यवान चतुर परन्तु समय का मारा रक्ष संस्कृति का प्रतिनिधि था। अब कोई उपाय नहीं देख, अपने परिवार के साथ पुलस्त्य पुत्र विश्रवा के आश्रम में आ गया। उसके साथ उसकी युवा पुत्री भी थी। जो अत्यन्त सुन्दर, चतुर, कार्य करने में दक्ष एवं प्रतिभा सम्पन्न लड़की थी। आश्रम में रहते-रहते ऋषि विश्रवा उस लड़की पर आसक्त हो गये। जबकि इसके लड़के की लड़की भी इससे उम्र में बड़ी थी। खुद कुबेर इन्हीं का लड़का लंका का प्रमुख बना बैठा था। इसी से कहा गया है कि जब तक व्यक्ति मानसिक रूप से संन्यास ग्रहण नहीं करता, मानसिक रूप से परमात्मा-प्रेमी नहीं बनता तब तक काम का रूपान्तरण ब्रह्मचर्य में होता ही नहीं। कपड़ा लाल, काला, पीला पहनने, दाढ़ी बढ़ा लेने से संन्यासी की आकृति तो ग्रहण कर लेते हैं परन्तु अन्दर से बकरा ही बने रहते हैं। बकरा काम का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वह भी दाढ़ी रखता है ऋषिवत्। काम के मामले में वही एक पशु है जो माँ, बहन, पुत्री को भी नहीं पहचानता। सम्भवत: बकरा इस पृथ्वी पर देवर्षि परम्परा का ही प्रतीक है। खैर उनकी आसक्ति को देख लड़की कैकशी, का चिन्तित होना स्वाभाविक था। कैकशी अपने पिता से सारी स्थिति कह देती है। पहले तो वे भी इनके आचरण पर भयभीत होते हैं परन्तु परिस्थिति का मारा व्यक्ति जब विघ्न-बाधाओं से युद्ध की हिम्मत छोड़ देता है। समझौतावादी हो जाता है। अतएव माल्यवान सोचने लगता है कि देवतागण जहाँ पराजित होते हैं वहाँ के राजा से रक्त सम्बन्ध कर अपनी स्थिति मजबूत करते आ रहे हैं। सम्भवतः यही कारण है कि इनका विकास तेजी से हो रहा है और हमारी संस्कृति समाप्त सी होती जा रही है। प्रातः काल वह प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री को सारी स्थिति से अवगत कराते हैं। पिता पुत्री को विश्रवा को वरण करने की सलाह देता है। रूपसी कैकशी ने यह बात पिता के मुँह से सुनने की कल्पना तक नहीं की थी। परन्तु पिता के द्वारा बार-बार समझाया जाता है कि समय से समझौता करने तथा अपना भविष्य बनाने के लिए कुछ कुर्बानी भी करनी पड़ती हैं। भविष्य के लिए वर्तमान से समझौता करना ही श्रेयस्कर है कैकशी। इस तरह उन्होंने कैकशी को समझा-बुझाकर तैयार किया।
कैकशी एवं विश्रवा
जब कैकशी के पिता ऋषिवर विश्रवा से शादी का प्रस्ताव रखते हैं तो वे भावविह्वल हो जाते हैं। मानो उनकी चिर-प्रतीक्षित इच्छा पूरी हुई। देवर्षि विश्रवा चौथे-पन में युवा लड़की कैकशी से शादी करते हैं। अब ऋषि कैकशी की सेवा से प्रसन्न थे। सदैव वह उनकी छाया के सदृश रहने लगी। आश्रम के प्रत्येक कार्य में हाथ बंटाने लगी। धीरे-धीरे वह इतनी महत्वपूर्ण हो गयी कि ऋषिवर उसकी इच्छा के बिना कोई कार्य ही नहीं करते। नीति नियमन में भी वह अहम् भूमिका निभाने लगी। माल्यवान यह देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। देवनीति ही उसके काम आयी। देवगण के नाश हेतु भविष्य उज्जवल नजर आया। समयानुसार अपनी पुत्री को उचित शिक्षा भी देता एवं भविष्य के प्रति सदैव सजग भी करता। लगन, निष्ठा एवं चतुरतापूर्वक किया गया निर्णय रंग लाया। समयानुसार उसे तीन पुत्र एवं एक पुत्री भी हुई। रावण बड़ा था। वह अत्यन्त सुन्दर, होनहार पैदा हुआ। जिसे देखकर देवर्षि मुग्ध हो गये। दूसरा लड़का विभीषण यह भी सुन्दर चतुर एवं भक्त प्रवृत्ति का था। तीसरा कुम्भकरण। यह भी सुन्दर, सुशील अपने से बड़ों का आदर करने वाला हुआ। परन्तु कुछ आलसी हो गया। लड़की स्वर्ण रेखा यानी अत्यन्त सुन्दर शरीर वाली थी। इसका शरीर मानो सोने की बनी हुई मूर्ति थी। इसी से इसे स्वर्णरेखा कहा गया। चौथा पुत्र खरदूषण का जन्म हुआ। यह भी कहीं-कहीं ज्ञात होता है कि अत्यन्त शक्तिशाली निर्भीक, बहादुर था। यह एकान्तप्रिय था। सम्भवतः इसीलिए यह दण्डकारण्य में तप-ध्यान में ज्यादा समय देता था। स्वर्णरेखा भी इसी के आश्रम में रहने लगी थी। चार भाई एवं एक बहन आपस में मिलकर रहते, विद्याध्ययन करते, युद्ध कला सीखते। रावण इतना तीव्र बुद्धि था कि वह एक साथ दस-दस कलाओं को ग्रहण करने में सक्षम हो गया। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि दस दिशाओं को पराभूत कर रही थी। शीघ्र ही उसने चार वेद, छह शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण कर लिया। किसी भी विद्या को या श्रुति के ऋचा को एक बार सुन लेने पर उसे याद हो जाता। उसकी प्रतिभा, स्मरणशक्ति को देखकर देवर्षि ने सहसा कह दिया कि तुम्हारी कीर्ति दसों दिशाओं में फैलेगी। तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि मानो दसानन है। इस तरह इसे दशानन कह दिया गया। दशानन में अपने पिता की तरह वाक्पटुता, सुन्दरता, विद्वता, चारित्रिक गुण आ गया। चूँकि उसके पिता देवगुणों से परिपूर्ण ऋषि थे। देवगुणों से परिपूर्ण देवर्षि अपने को उत्तम कुल के कहते थे। दशानन की प्रतिभा, तप एवं राज्य करने की आकांक्षा मातृ प्रधान हो गयी। यानी माता का गुण उसमें आ गया। चूँकि उसकी माता रक्ष संस्कृति की थी। इसी तरह से विभीषण भी पिता के अनुरूप सुन्दर विद्वान तो हुआ परन्तु चारित्रिक गुण माँ पक्ष से उसे मिला। इस तरह विभीषण में भक्तित्व का प्रधान होना मातृपक्ष के चलते सहज हो गया चूंकि उसकी माँ परमभक्त, पतिव्रता एवं दृढ़ चरित्र की थी। बचपन से विभीषण में
देवजन्य गुण कम एवं रक्ष तथा मानव संस्कृति के गुण ज्यादा आये। परमपिता परमात्मा के सामने अपने को समर्पित करने की भावना ज्यादा रही। साथ ही पद लोलुपता, तड़क-भड़क का जीवन, वाक्पटुता इसे देव संस्कार से मिली। इसी से इसका नाम विभीषण रखा गया।
कुम्भकरण यानी कुम्भ की तरह जिसका कर्ण या कान हो, यह किसी भी विद्या को शीघ्र ग्रहण करता था। किसी भी शस्त्र को अपने में कुम्भ यानी घड़े की तरह स्थिर रखता था। इसकी बुद्धि धीर, गम्भीर एवं अनुशासित थी। इसके शरीर की बनावट उसके नाना पर और बुद्धि उसकी माँ पर, जो अत्यन्त वीर थी। यह गम्भीर विचार वाला किसी भी विद्या को कुम्भ की तरह रखने वाला हुआ। इसलिए देवर्षि ने इसका नाम कुम्भकर्ण रखा।
स्वर्णरेखा इसकी सुन्दरता माँ और बाप से मिलती-जुलती एवं दोनों से अच्छी थी। सेवा की भावना माँ की तरफ से आयी। चारित्रिक गुण, विद्या, जीने की शैली यह पिता की तरफ से मिल गयी। इसी से उसका नाम स्वर्णरखा रखा। देवतागण उसकी वाक्पटुता, कार्यक्षमता एवं विद्वता देखकर मोहित हो गये।
क्रमशः..